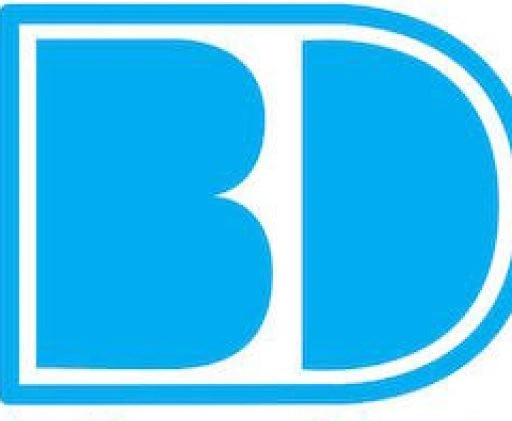जब भी कोई ये कहता है कि सत्यजीत रे की फिल्में उन्हें बोरिंग लगती है तब मुझे दुःख ज़रूर होता है मगर मैं उन लोगो से किसी भी तरह की बहस नहीं करता। मैं यह सोचकर, मुस्कुराते हुए, वहाँ से उठकर चला जाता हूं की या तो इस व्यक्ति ने कभी भी सत्यजीत रे की फिल्में देखी ही नहीं या फिर ये भी मसालेदार सिनेमा की भेट चढ़ गया है।
सत्यजीत रे पर शुरू से ये आरोप लगते रहे की उन्होंने भारत की गरीबी बेच दुनिया भर से अवार्ड बटोरे है। ये बात अलग है की उनकी बनाई गयी सभी फिल्मो में सिर्फ किन्ही दो फिल्मो में गरीबी की दशा को दिखाया गया है। एक दफा जब उनसे किसी पत्रकार ने इस आरोप पर टिप्पणी मांगी तो उन्होंने मुस्कुरा कर बोल दिया की उन्हें कुछ नहीं कहना क्योंकि उन्हें कुछ भी बुरा नहीं लगा। इस देश में सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी है।
सत्यजीत रे को सिर्फ उनकी फिल्में महान नहीं बनाती। उनके महान होने का कारण यही सादापन और ज़मीनी स्वाभाव था। दूसरे के विचार को जगह देने की क्षमता जो आज हम में से शायद किसी के पास नहीं है।
आप सोच रहे होंगे की आज अचानक सत्यजीत रे की बात कहा से करने लगा। तो ये भी साथ में बताता चलू की ‘पाथेर पांचाली’ इस वर्ष अपने 60 वर्ष पूरे कर रही है। यह फ़िल्म उन चुनिंदा फिल्मो में से एक है जो अपने आप में एक फ़िल्म स्कूल है। न जाने कितने ही फ़िल्मकार, कथाकार फिल्मो की दुनिया में आये इस फ़िल्म को देखने के बाद। मैंने पहली बार ‘पाथेर पांचाली’ भोपाल स्थित भारत भवन में देखी थी। इस महान फ़िल्म को उस कमाल के माहौल में देखना एक अद्भुत अहसास था। इटैलियन निओरीलिस्म से प्रभावित रे ने जब 1950 में ‘पाथेर पांचाली’ बनाने के बारे में सोचा था तब उन्हें भी नहीं पता था की यह फ़िल्म वैश्विक स्तर पर इतना बड़ा मुकाम हासिल करेगी।
 मैं मानता हू की यह एक ऐसी फ़िल्म है जिसका कोई एक दर्शक वर्ग नहीं। बहुत से लोग इस फ़िल्म को देखने से इसलिए कतराते है, जैसा की मैंने देखा है, क्योंकि उन्हें लगता है की यह एक अति गंभीर विषय पर बनी ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म है। हालांकि ये बात सच भी है लेकिन एक अच्छा निर्देशक बहुत ही खूबसूरती से एक गंभीर कहानी को भी ऐसे प्रस्तुत करता है की सभी उस फ़िल्म का आनंद उठा सके। सत्यजीत रे तो फिर भी एक महान निर्देशक थे।
मैं मानता हू की यह एक ऐसी फ़िल्म है जिसका कोई एक दर्शक वर्ग नहीं। बहुत से लोग इस फ़िल्म को देखने से इसलिए कतराते है, जैसा की मैंने देखा है, क्योंकि उन्हें लगता है की यह एक अति गंभीर विषय पर बनी ब्लैक एंड वाइट फ़िल्म है। हालांकि ये बात सच भी है लेकिन एक अच्छा निर्देशक बहुत ही खूबसूरती से एक गंभीर कहानी को भी ऐसे प्रस्तुत करता है की सभी उस फ़िल्म का आनंद उठा सके। सत्यजीत रे तो फिर भी एक महान निर्देशक थे।
दरअसल, मैंने भी इसी पूर्वाग्रह के साथ ‘पाथेर पांचाली’ देखनी शुरू की थी। मगर जैसे ही आधा घंटा बीता होगा, मेरा नजरिया बदलने लगा। एक दस साल के बच्चे के लिए भी इसमें रस है और एक 70 साल के बुजुर्ग के लिए भी। इन दोनों ही दर्शको को ये फ़िल्म उतनी ही पसंद आएगी। यह भी सच है की इन दोनों दर्शको के लिए यह फ़िल्म अलग-अलग स्तर पर खुलेगी मगर प्रभाव दोनों पर एक जैसा ही होगा।
शायद तभी हम इस फ़िल्म को क्लासिक का दर्जा देते है।
यूँ तो फ़िल्म का प्रत्येक दृश्य लुभावना है। चाहे वो क्लाइमेक्स हो जब दुर्गा बिस्तर पर बीमार पड़ी रहती है और माँ बगल में बैठी गरम पानी में भिगोई पट्टी दुर्गा के माथे पर लगाती है। बाहर ज़ोरो से चल रही आंधी ऐसा मानो सब कुछ तबाह कर देना चाहती हो। दिया आंधी से लड़ते-लड़ते बुझ जाता है। आंधी मानो दरवाज़ा तोड़ के घर के अंदर घुस जाना चाहती हो। जैसे की आंधी न हो गरीबी हो जो सब कुछ तबाह कर देना चाहती है। यह दृश्य इतना डरावना है की आप इसके ख़त्म होने का इंतज़ार करते रहते है। मगर जब ये ख़त्म होता भी है तो दर्द के साथ। बेटी के मर जाने का दर्द।
जो दृश्य मुझे सबसे प्यार लगा वो था जब दुर्गा अप्पू को पहली बार ट्रेन दिखाने काश के फूलो के खेतो में ले जाती है। अप्पू की आँखों की ख़ुशी देख के आप समझ जाएंगे की बचपन क्या होता है। मै यह सोचकर दंग रह जाता हूं की ट्रेन की आवाज़, उसका गुज़रना, मुझे क्यों इतना रोमांचित करता है। शायद उस वक्त, मै भी अप्पू बन जाता हू।
जिस दृश्य की मैंने ऊपर बात की उस दृश्य को फिल्माने में कितनी मेहनत और लगन लगी थी, ये जानने के बाद आप चकित रह जाएंगे। दरअसल, ये सबसे पहला दृश्य था फ़िल्म का जो शूट हुआ था। सत्यजीत रे उस वक्त एक दूसरी नौकरी भी करते थे। उन्हें सिर्फ शनिवार और रविवार का वक्त मिला करता था फ़िल्म शूट करने के लिए। अपनी पूरी टीम को लेकर वे अप्पू और ट्रेन वाला दृश्य फिल्माने काश के फूलो के खेत पहुच गए थे। उस एक दिन उन्होंने काफी कुछ सीखा मगर दृश्य के कुछ भाग अब भी फिल्माने रहते थे। जब वे दूसरे हफ्ते वहा शॉट पूरा करने पहुचे तो देखा की पशुओ ने सारा खेत तहस-नहस कर दिया है। कॉन्टीनुइटी टूट जाती इसलिए उन्हें अगले मौसम का इंतज़ार करना पड़ा था ताकि फूल दोबारा खिले। ऐसा ही हुआ और तब जाकर ये दृश्य पूरा हो पाया।
सोचिए! इतना परिश्रम, धीरज सिर्फ एक दृश्य को फिल्माने के लिए। ‘पाथेर पांचाली’ को लगभग तीन वर्ष लग गए पूरा होने में। जिसमे से दो वर्ष से अधिक तो निर्माताओ को खोजने में ही बीत गए। फ़िल्म शूट होती और फिर पैसो के कमी के काऱण रुक जाती।
बलिदान किसी कहते है यह सिर्फ सत्यजीत रे या फिर उनकी पत्नी अच्छी तरह बता पाती। फ़िल्म बनाने में उन्हें अपने गहने भी बेचने पड़े। कुछ सालो के बाद पश्चिम बंगाल की सरकार ने फ़िल्म फाइनेंस करने की बात मान ली। मगर ये पैसा भी किश्तों में ही मिलता।
इन सभी समस्याओ के बावजूद सत्यजीत दा की सबसे बड़ी चिंता पैसा नहीं था।वे इस बात से ज़्यादा चिंतित थे की अप्पू और दुर्गा बड़े हो रहे थे। उन्होंने बहुत साल बाद एक साक्षात्कार में बताया, “यह एक चमतकार ही था की तीन सालो तक अप्पू की आवाज़ में कोई बदलाव नहीं आया। दुर्गा बड़ी नहीं हुई। और इन्दिर मरी नहीं।”
सत्यजीत रे के परिश्रम, सहनशीलता, धीरज और प्यास ने वक्त को जैसे रोक लिया था।
‘पाथेर पांचाली’ पर देश की गरीबी को बेचने का आरोप आज भी बहुत लोगो को सही लगता है मगर एक देश जब कंगाली और भुखमरी के दौर से गुज़र रहा हो। उसके लोगो के पास पहनने को कपडे न हो और खाने को रोटी न हो, उस दौर में एक फिल्मकार अपनी फिल्मो के द्वारा कौन सी अमीरी दिखाएगा? और अगर वह दिखा भी देता है एक ऐसी दुनिया जहा कोई कष्ट नहीं है, दुःख नहीं है तो क्या तब भी आप सिनेमा को समाज का आईना कहेंगे। मुझे लगता है हमे आईने को अब साफ़ कर लर्न चाहिये। इस पर धूल जम गयीं है ।
Written By: Shubham Pandey