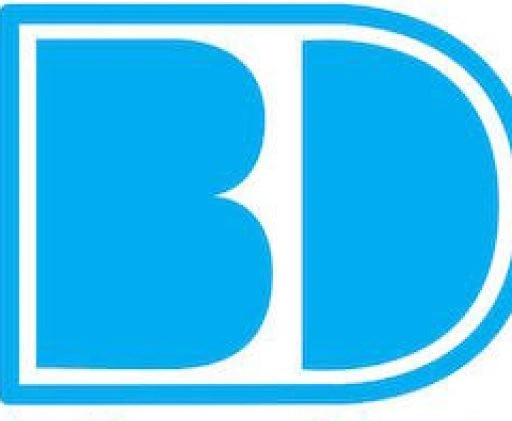कहते हैं “किसी को अगर जानना हो तो उसकी दिनचर्या के बारे में पता लगाओ, देखो वो अपने जीवन की छोटी छोटी चीज़ों को कैसे करता है। और आपको पता चलता है कि उसका चरित्र कैसा है। “कोर्ट” देखते वक़्त भी कुछ ऐसा ही महसूस हुआ। पारम्परिक सिनेमा के स्ट्रक्चर से अलग हट कर हर किरदार के साथ उसके पर्सनल स्पेस में जाती यह फिल्म उनके बारें में बहुत कुछ दिखाती है।
कोर्ट न तो सिर्फ कोर्ट के बारे में है, और न ही इसके मुख्य किरदार नारायन कांबले के बारे में। यह फिल्म हमारे बारे में है,हमारे बीच के किरदारों के बारे में। चाहे वो पब्लिक प्रॉसिक्यूटर जो कोर्ट से घर जाते हुए रास्ते में कॉटन साड़ी और ओलिव आयल की बात करती है, घर पर जाकर डेली सोप देख रहे पति के लिए खाना बनाती है। या फिर डिफेंस लॉयर जो कोर्ट के बाद एक सुपर मार्किट में शॉपिंग करते हुए रोज़मर्रा की ज़रूरतों के सामान से लेकर शराब तक की खरीददारी करता है और पार्लर में फेशियल करवाता है। या फिर वो कोर्ट का जज जो एक महिला के केस की सुनवानी इसलिए नहीं करता क्योँकि उसने स्लीवलेस टॉप पहना हुआ है।
कई बार फिल्म देखते हुए ये भी लगता है कि इस सीन की क्या ज़रुरत थी, ये तो नारायन कांबले का केस से नहीं जुड़ा, पर कुछ आपको पता चलने लगता है कि नारायन कांबले का केस तो एक जरिया है जिसकी ऊँगली पकड़ कर कोर्ट के वो कोने तलाशे जा रहे हैं, जिसके अंदर शायद हम अपना दिमाग रख कर भूल गए है। और उसके कारण हम कांबले के गाने में छिपे मेटाफोर को न समझ कर एक सीवर सफाईकर्मी की मौत की ज़िम्मेदारी हम उसके ऊपर मढ़ने लग जाते हैं| जबकि मौत की वजहें कुछ और ही हैं। उस सफाई कर्मचारी की बीवी से पूछे जाने वाले सवाल के दौरान कैमरा सिर्फ उसी का चेहरा दिखाता है और अपने पति के मौत के बारे में वो हर सवाल का ऐसे जवाब देती है जैसे कोई आम सी बात है। वो जानती है कि हर सीवर साफ़ करने वाले की मौत शायद ऐसी ही होती है। ये सीन हमारे समाज की विसंगतियों पर एक तमाचा है। ठीक उसके बाद जब डिफेन्स लॉयर जाते हुए वो अपने काम की बात करने लगती है। उसके पति की मौत उसके लिए स्वीकार्य हैं।

दूसरी तरफ एक किताब लिख देने पर या सरकार की नीतियों के खिलाफ गाना गा देने पर नारायन कांबले को गिरफ्तार कर लिया जाना हमारी सरकार की तानाशाही का सूचक तो है ही, साथ ही साथ यह एक तरीका भी है जिससे ये बताया जा सकता है कि हम तुम्हारे आका है और ये सारे नियम हमारे हैं, इसमें रहना है तो हमारे हिसाब से रहना पड़ेगा।
फिल्म के कुछ जिरह के सीन ये सवाल भी लेकर आते हैं कि आखिर हम कब तक अंग्रेज़ों के जमाने के बने हुए कानून के हिसाब से लोगों को सजा देते रहेंगे। दूसरी तरफ किस तरह हम लोगों ने लिखी हुई चीज़ को पत्थर की लकीर मान लिया है। हमारी सोच उस पैराग्राफ के पहले शब्द से शुरू होती है और आखिरी शब्द तक जाते जाते समाप्त हो जाती है। और आखिर हो भी क्यों ना क्योंकि हमारे पास और कुछ सोचने का टाइम ही नहीं है क्योंकि हमारा इवनिंग टाइम एंटरटेर्मेंट भी मराठी मानुस के अहम को बढ़ावा देना में जाता है या फिर किसी पब में बैठ कर गप्पियाने में।
आखिरकार जब कोर्ट एक महीने के लिए बंद होता है, तब तक नारायन कांबले के केस का फैसला नहीं हुआ होता और अब उसको एक महीना जेल में ही रहना होगा। उसके बाद भी उसका क्या होगा पता नहीं शायद इसीलिए उस सीन में सारी लाइट्स धीरे धीरे बंद होती है और दर्शक को अन्धकार में छोड़ती हैं।
दूसरी तरफ वेकेशन के लिए वही जज अपने दोस्तों के साथ शहर के पास के रिज़ॉर्ट में जाता है और वहाँ अपने दोस्त को उसके बेटे के बोलने के लिए सलाह देता दिखता है कि “इसे अंगूठी पहनाओ तब जाकर ये बोलने लगेगा”, वो आईआईएम और आईआईटी में मिलने वाले पैकेज की बात करता है। इस तरह फिल्म हमें उस जज के पर्सनल स्पेस में भी ले जाती है और दिखाती है कि जिन्हें हम सबसे समझदार और दिमाग वाला मानते हैं और शायद इसी वजह से हमारे समाज के बड़े फैसलों पर निर्णय लेने का अधिकार उन्हें देते हैं उनकी खुद की बुद्धि कैसी है।
फिल्म देख कर थोड़ा गुस्सा आना तो लाजमी हैं| पर ये सोच कर मैं भी करुणा से भर जाता हूँ कि जैसे हम हैं न … बस आप समझ जाइये|
Written By:- Neeraj Pandey {@getneerajpandey}